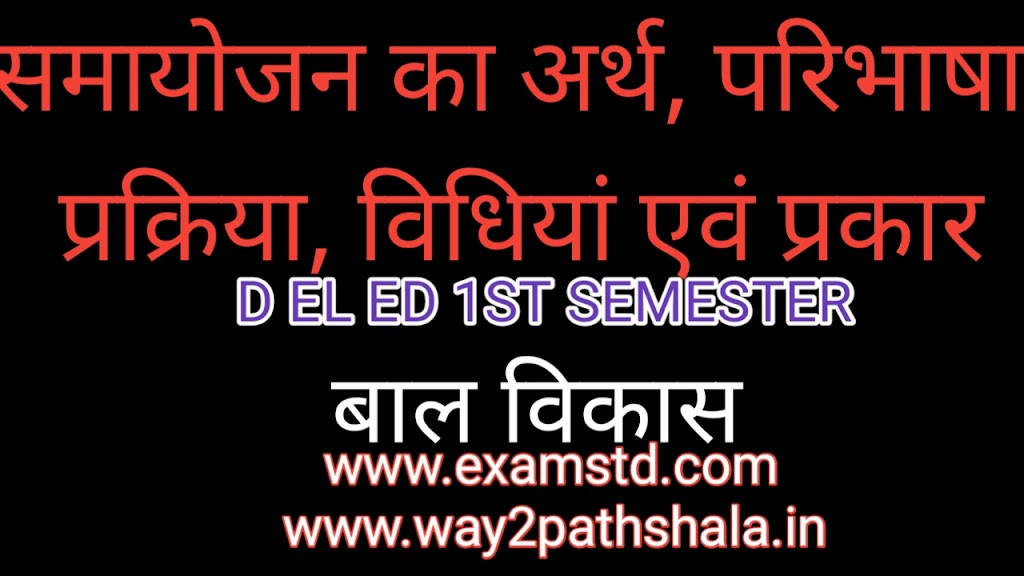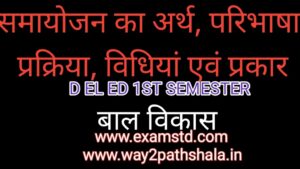समायोजन का अर्थ, परिभाषा, प्रक्रिया, विधिया, प्रकार, विशेषताएं एवं लक्षण d el ed notes | bal vikas notes in hindi
www.way2pathshala.in , तथा www.examstd.com के द्वारा BTC/DELED 1st Semester, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया (प्रथम प्रश्न पत्र) के पाठ-3 व्यक्तित्व का विकास, उनका अर्थ एवं प्रकार के अंतर्गत समायोजन का अर्थ, परिभाषा, प्रक्रिया, विधिया, प्रकार विशेषताएं एवं लक्षण d el ed notes | bal vikas notes in hindi को आप के समछ लाया गया है।
समायोजन का अर्थ क्या होता है?
समायोजन दो शब्दों को मिलाकर बना है-सम और आयोजन। सम् का अर्थ है भली-भाँति, अच्छी तरह या समान रूप से और आयोजन का अर्थ है व्यवस्था अर्थात् अच्छी तरह व्यवस्था करना। समायोजन का अर्थ हुआ सुव्यवस्था या अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकताएँ पूरी हो जाए और मानसिक द्वन्द्व न उत्पन्न होने पाये।
गेट्स एवं अन्य विद्वानों अनुसार – ‘समायोजन’ शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ में निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं और पर्यावरण के
बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध् रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन कर देता है। दूसरे अर्थ में समायोजन एक संतुलित दशा है जिस पर पहुँचने पर हम उस व्यक्ति को सुसमायोजित कहते हैं। एक छात्र अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना अपना लक्ष्य बनाता है, पर दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता और अपनी कम योग्यता के कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है। इससे वह निराशा और असन्तोष, मानसिक तनाव और संवेगात्मक संघर्ष का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में वह अपने मौलिक लक्ष्य को त्यागकर अर्थात् अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अपनी असफलता के प्रति ध्यान न देकर वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना अपना लक्ष्य बनाता है। अब यदि वह अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो वह अपनी परिस्थिति या वातावरण से ‘समायोजन‘ कर लेता है।पर यदि उसे सफलता नहीं मिलती है, तो उसमें ‘असमायोजन‘ उत्पन्न हो जाता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिस्थितियांे
को अनुकूल बनाना या परिस्थितियों के अनुकूल हो जाना ही समायोजन कहलाता है। यह समायोजन व्यक्ति अपनी क्षमता, योग्यता के अनुसार करता है।
समायोजन और असमायोजन के अर्थ को निम्न प्रकार से स्पस्ट करसकते है
बोरिंग,लैंगफेल्ड व वेल्ड के अनुसार- “समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परस्थितियों में संतुलन रखता है |
गेट्स व अन्य के अनुसार-
समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलन सम्बन्ध रखने के लिए अपने वयवहार में परिवर्तन करता है
समायोजन की परिभाषा
बोरिंग,लैंगफील्ड एवं वैल्ड के अनुसार- ‘’समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को
प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है।’’
स्किनर के अनुसार- “समायोजन शीर्षक के अंतर्गत हमारा अभिप्राय इन बातों से है सामूहिक क्रियाकलापों में स्वस्थ तथा उत्साहमय ढंग से भाग लेना, समय पड़ने पर नेतृत्व का भार उठाने की सीमा तक उत्तरदायित्व वाहन करना तथा सबसे बढ़कर समायोजन में अपने को किसी भी प्रकार का धोखा देने से बचने की कोशिश करना”
स्मिथ के अनुसार -“अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित तथा संतोष देने वाला होता है”
गेट्स व अन्य – ‘‘समायोजन निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित सम्बन्ध रखने के लिए
अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है।‘‘
कोलमैन के अनुसार– “समायोजन व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कठिनाइयों के निराकरण के प्रयासों का परिणाम है”
इन परिभाषाओं से स्पष्ट हैकि समायोजन निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही व्यक्ति, परिस्थिति तथा पर्यावरण के मध्य अपने को समायोजित करने के लिये अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अतः समायोजन को संतुलित दशा कहा गया है।
समायोजन की प्रक्रिया
समायोजन के स्वरूप को समझने के बाद हमारे लिए आवश्यक है कि हम समायोजन की प्रक्रिया को समझ ले इसके अध्ययन के बाद हम सुसमायोजित व्यक्तियों को शिक्षा की सहायता से उत्पन्न करनेमें समर्थ हो सकेंगे समायोजन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी सहायता से व्यक्ति का जीवन अपने आप पर्यावरण के मध्य अधिक बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है
समायोजन की प्रक्रिया की सात अवस्थाएं होती है
- प्रथम अवस्था-उत्तेजना महसूस करना (अपूर्व आवश्यकताओं के कारण आंतरिक या बाह्य या दोनों के द्वारा उत्तेजना का अनुभव)
- द्वितीय अवस्था-द्वंद (आवश्यकताओं के पूर्ण न होने पर द्वंद का अनुभव)
- तृतीय अवस्था-तनाव (द्वंद की मानसिक दशा से तनाव की उत्पत्ति)
- चतुर्थ अवस्था-तनाव के लक्षण का प्रकट होना (तनाव के शारीरिक और मानसिक लक्षणों का प्रकट होना पीड़ाग्रस्त एवं बेचैन रहना)
- पंचम अवस्था-प्रयास ( अपनी बेचैनी और पीड़ा को कम करने का प्रयास)
- छठी अवस्था-उन्मोचन (आवश्यकताओं की संतुष्टि से तनाव कम होना)
- सातवीं व्यवस्था-समायोजन ( उन्मोचन के आधार पर व्यक्ति स्वयं से तथा अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करता है )
समायोजन की विधियां
समायोजन की दो विधियां होती हैं
- प्रत्यक्ष विधि
- अप्रत्यक्ष विधि
समायोजन की प्रत्यक्ष विधि- प्रत्यक्ष विधियां वे विधियां हैं जिनके द्वारा बालक अथवा व्यक्ति चेतन अवस्था में अपने मानसिक तनाव को दूर करने का प्रयास करता है इन विधियों में वह अपनी तर्क एवं चिंतन शक्ति का प्रयोग करता है इन प्रत्यक्ष विधियों के कुछ उपाय निम्न हैं
- प्रयत्न में सुधार– इस विधि में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न
करता है वह अपने लक्ष्य में आने वाली बाधाओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करता है और उन बाधाओं को हटाने का प्रयास करता है इससे वह तनावों से मुक्ति पाता है - अन्य मार्ग खोजना- इस विधि में व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली रुकावटें और बाधाओं को अनेक प्रयत्न द्वारा दूर नहीं कर पाता है तो वहां
उसी के समरूप एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करता है जो उसकी इच्छा को संतुष्टि दे सके और वहां उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है लक्ष्य प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने पर मानसिक तनाव दूर होता है - समर्पण-जब कोई व्यक्ति अपने सारे प्रयत्नों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता तो वहां नियति मानकर एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करता है जिससे
जिसे वह आसानी से प्राप्त कर सके और कम प्रयासों में उसे प्राप्त हो जाए वह उसी से प्रसन्न होकर अपने आप को संतुष्ट कर लेता है - विश्लेषण एवं निर्णय– जब किसी व्यक्ति के सामने परस्पर विरोधी एक से अधिक लक्ष्य होते हैं तो वह निर्णय नहीं कर पाता कि वह किसे स्वीकार करें और किसे छोड़ दे इस विधि में वह अपने सामने उपस्थित सभी परिस्थितियों, क्षमताओं तथा योग्यताओं का विश्लेषण करता है और गुण एवं दोषों की विवेचना करके किसी एक लक्ष्य को चुन लेता है|
समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां –अप्रत्यक्ष विधियां वे विधियां हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप में अपनाता है तनाव से उत्पन्न दुखद अनुभूतियों से बचने के लिए व्यक्ति के अचेतन मन में कुछ प्रक्रिया चलती हैं जो स्वत: ही हो रही होती हैं व्यक्ति को इनका ज्ञान नहीं होता है इन प्रक्रियाओं को वह अपने मन में कल्पना के
द्वारा चलाता रहता है इसके द्वारा उसका तनाव अस्थाई रूप से कम हो जाता है अप्रत्यक्ष विधियों के कुछ उपाय निम्न हैं
- दमन-दमन का अर्थ है किसी चीज को दबा देना। कभी-कभी व्यक्ति कुछ इच्छाओं को कई कारणों की वजह से पूरा नहीं कर पाता तो वह उन इच्छाओं अथवा कामनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं होने देता और उन इच्छाओं को अपने अचेतन मन में धकेल देता है
- प्रतिगमन-प्रतिगमन का अर्थ हैं। पीछे लौटना इसमें व्यक्ति अपने दुख तनाव असंतोष से मुक्ति पाने के लिए अपने पूर्व अनुभव और प्रक्रियाओं की ओर लौट जाता है जिन्हें वह बाल्यावस्था में किया करता था जैसे- व्यक्ति कभी-कभी असफल होने पर बच्चों जैसा व्यवहार करता है जैसे- चिल्लाना, पैर पटकना, रोना आदि
- शोधन-शोधन का अर्थ होता है शुद्ध करना। मनोवैज्ञानिक भाषा में शोधन को एक युक्ति के रूप में प्रयुक्त किया गया है जिसका तात्पर्य है अचेतन की वह मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति की अवांछनीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को कृतिम पक्ष की ओर मोड़ दिया जाता है जिसे समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है जैसे- किसी व्यक्ति द्वारा अपनी काम प्रवृत्ति को कला और दर्शन की ओर मोड़ देना
- पलायन- पलायन का अर्थ है पीछे हटना। इस युक्ति में व्यक्ति दुख और तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से अपने आपको अलग कर लेता है जैसे- किसी विद्यार्थी का किसी विद्यालय में किसी समूह द्वारा मजाक बनाने या अवहेलना करने पर कई बार विद्यार्थी विद्यालय को बदल देते हैं
- दिवास्वप्न- दिवास्वप्न का अर्थ होता है काल्पनिक जगत में रहना। इसमें व्यक्ति अपनी दुखद अनुभूतियों से निजात पाने के लिए वर्तमान से हटकर कल्पना लोक में विचरण करने लगता है और उसे सुख की अनुभूति होती है दिवास्वप्न द्वारा वह अपनी असफलताओं एवं तनाव की स्थितियों को सफलता एवं सुखद स्थितियों में बदल देता है और कुछ समय के लिए संतोष एवं सुख का अनुभव करता है
- एकरूपता- एकरूपता का अर्थ है किसी के जैसा समझना। इसमें व्यक्ति द्वारा अपनी असफलता को छुपाने के लिए किसी सफल व्यक्ति के गुणों एवं
कृतियों को अपने में दिखाने की कोशिश करता है जैसे- कोई बालक अपने अवगुणों को छुपाने के लिए कहता है कि मैं उन अमुक विद्वान का पुत्र हूं।
समायोजन की विशेषताएं
समायोजन करने वाले व्यक्ति में विभिन्न विशेषताएं होती हैं। इन्हीं विशेषताओं का अध्ययन इस प्रकार से किया गया है –
- ये पूर्णतया संतुलित रहते हैं। इनके स्पष्ट उद्देश्य होते हैं।
- ये अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर लेते हैं।
- इन्हें हमेशा परिस्थिति का ज्ञान होता हैं।
- ये अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट एवं सुखी रहने वाले होते हैं।
- ऐसे व्यक्ति समाज के प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखने वाले होते हैं।
- ये संवेगात्मक रूप से स्थिर होते है।
- ये व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं।
- ऐसे व्यक्ति अपनी गल्तियों का दोषारोपण दूसरों पर नहीं करते।
समायोजन के लक्षण
समायोजन करने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते है
- संतुष्टि एवं सुख
- समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान
- संतुलन
- सामाजिकता, आदर्श चरित्र , संवेगात्मक रूप से अस्थिर, संतुलन एवं दायित्वपूर्ण
- परिस्थिति का ज्ञान , नियंत्रण तथा अनुकूल आचरण
- पर्यावरण तथा परिस्थिति से लाभ उठाना
गेट्स के अनुसार-“समायोजित व्यक्ति वह है जिसकी आवश्यकताएं एवं तृप्ति सामाजिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की स्वीकृति की साथ संगठित
हो”
इन्हे भी पढ़े 👇👇👇